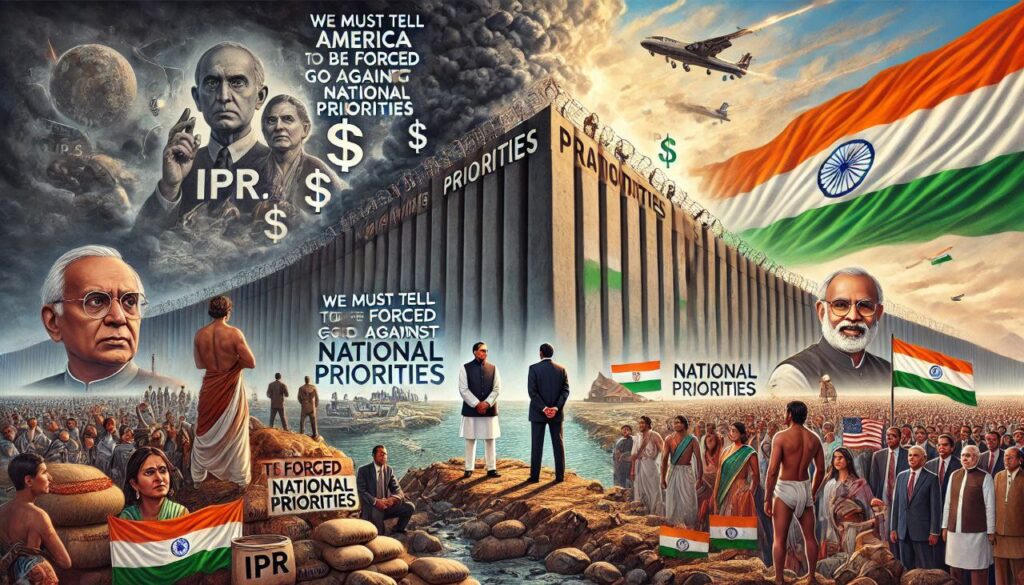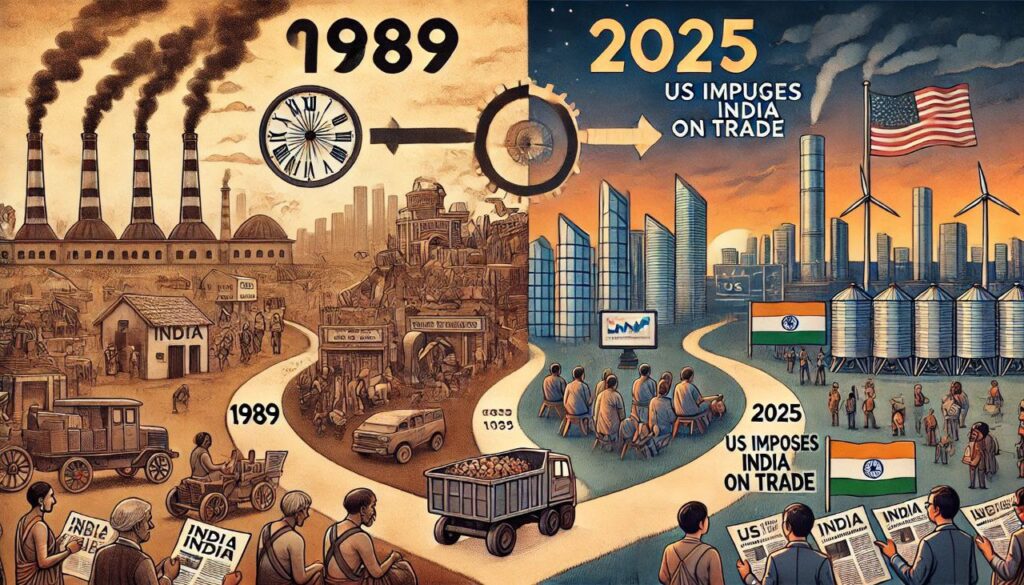ज़रा एक पल के लिए आँखें बंद करिए और कल्पना कीजिए… सुबह का वक्त है। टीवी पर फ्लैशिंग हेडलाइंस चल रही हैं—“अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ़ लगा दिए।” सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है—#Boycott US #India versus US। अख़बार की हेडलाइन चिल्ला रही है—“भारत पर व्यापारिक हमला।” आपके दिमाग़ में पहला सवाल यही उठेगा—आखिर क्यों बार-बार भारत ही निशाना बनता है?
हम वो देश हैं जिसे दुनिया “सबसे बड़ी लोकतंत्र” कहती है। हम वो देश हैं जो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था माना जाता है। हम वो देश हैं जिसने आईटी से लेकर अंतरिक्ष तक, मेडिसिन से लेकर स्टार्टअप्स तक दुनिया को चौंकाया है। फिर भी, हर दशक में, हर पीढ़ी में, अमेरिका का ‘व्यापारिक हथियार’ हमें ही भेदता क्यों है? आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे।
आपको बता दें कि अमेरिका का यह सवाल नया नहीं है। 2025 की यह हलचल हमें 35 साल पीछे, 1989 में ले जाती है। तब भारत का चेहरा अलग था, लेकिन हालात कुछ-कुछ वैसे ही थे। राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री रहे दिनेश सिंह ने अमेरिका के ‘Super 301’ पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था—“अमेरिका दोहरे मानदंडों का दोषी है और हर उस क्षेत्र में बाधाएँ खड़ी कर रहा है जहाँ हम Competition करते हैं।” यह बयान सुनते ही लगता है जैसे यह आज दिया गया हो। लेकिन हकीकत यह है कि यह बयान 1989 का है। यानी इतिहास जैसे खुद को दोहराता है।
अब सोचिए, उस दौर में अमेरिका किसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था? जवाब है—जापान। अस्सी के दशक में जापान की कारें, जापान का इलेक्ट्रॉनिक्स, जापान की टेक्नोलॉजी अमेरिकी बाज़ार पर छा रही थी। अमेरिकी मीडिया हेडलाइंस लिखती—“अमेरिका का जापानीकरण हो रहा है।” अमेरिकी राजनेता खुले मंच से कहते—“जापान हमारे पैसे से हमें ही खरीद रहा है।” यह गुस्सा अमेरिका की नसों में दौड़ रहा था। जापान के उदय ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। और यहीं से अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला—सुपर 301।
सुपर 301—नाम भले ही साधारण हो, लेकिन इसका असर हथियार से कम नहीं था। यह अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 का संशोधित रूप था, जिसे 1988 में राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने और ज़्यादा ताक़तवर बना दिया। इस कानून के तहत अमेरिका उन देशों की पहचान करता था जो ‘अनुचित व्यापारिक प्रथाओं’ में शामिल हैं। फिर उन पर भारी-भरकम टैरिफ़ और प्रतिबंध लगाए जाते। शुरुआत में इसका असली निशाना जापान था। लेकिन 1989 में जब अमेरिका ने अपनी पहली ‘सुपर 301 लिस्ट’ जारी की, तो उसमें तीन नाम देखकर भारत सकते में आ गया—जापान, ब्राज़ील और भारत।
अब सवाल यह था कि भारत इस लिस्ट में आया कैसे? जापान का अमेरिका से व्यापार Surplus अरबों डॉलर का था। ब्राज़ील भी एक बड़ी उभरती हुई ताक़त था। लेकिन भारत? भारत का Surplus तो महज़ 690 मिलियन डॉलर का था। फिर भी, अमेरिका ने हमें उसी लिस्ट में डाल दिया। इससे साफ़ था कि अमेरिका का मकसद सिर्फ़ ‘न्यायपूर्ण व्यापार’ नहीं था, बल्कि दबाव बनाना था। भारत से अमेरिका क्या चाहता था? जवाब साफ़ है—वह चाहता था कि भारत अपने दरवाज़े अमेरिकी बीमा कंपनियों, हॉलीवुड की फिल्मों, होम वीडियो और विदेशी कंपनियों के लिए पूरी तरह खोल दे। वह चाहता था कि भारत पेटेंट और कॉपीराइट कानूनों को सख़्त करे, ताकि हमारी जेनेरिक दवाओं पर रोक लगे।
उस समय भारत राजनीतिक रूप से उथल-पुथल से गुजर रहा था। बोफोर्स कांड के बाद राजीव गांधी की पकड़ ढीली पड़ गई थी और वी पी सिंह की सरकार आ चुकी थी। लेकिन दिलचस्प यह है कि दोनों नेताओं ने अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने से इंकार कर दिया। वी पी सिंह ने साफ़ कहा—“हमें अमेरिका को यह बता देना चाहिए कि हमें अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के खिलाफ़ जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।” यह बयान आज भी उतना ही Relevant है।
लेकिन अमेरिका की रणनीति देखिए। उसने भारत को लिस्ट में तो डाल दिया, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके अपने कानून के तहत पहले यह साबित करना ज़रूरी था कि, अमेरिकी कंपनियों को भारत की नीतियों से कितना नुकसान हुआ है। इस जांच में महीनों लग गए। और तब तक हालात बदल गए। 1991 में भारत ने पी वी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की अगुवाई में Economic liberalization का ऐतिहासिक फैसला किया। foreign investment के दरवाज़े खुले और अमेरिका की कई माँगें अपने-आप पूरी हो गईं।
अब सोचिए, यह कहानी कितनी दिलचस्प है। 1989 में भारत सुपर 301 की लिस्ट में आया, लेकिन अमेरिका तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाया। फिर 1991 में भारत ने अपनी नीतियाँ बदलीं। यह बदलाव अमेरिकी दबाव से था या हमारी मजबूरी से, यह बहस का विषय है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर अपने टैरिफ़ हथियार से हमें झुका दिया।
और यही पैटर्न आज 2025 में दोहराया जा रहा है। फर्क सिर्फ़ इतना है कि आज जापान की जगह चीन है। ट्रम्प ने चीन के खिलाफ़ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ही टैरिफ़ लगाकर की थी। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी थी। लेकिन अब ट्रम्प ने चीन पर थोड़ी नरमी दिखा दी है। क्यों? क्योंकि चीन पर सख़्ती से Global energy कीमतें और सप्लाई चेन गड़बड़ा सकती है। लेकिन भारत? भारत पर टैरिफ़ लगाना उनके लिए आसान है। क्योंकि इससे उन्हें एक साथ कई संदेश भेजने का मौका मिलता है—रूस को भी, चीन को भी और भारत को भी।
भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे परिष्कृत करके बेच रहा है। चीन भी यही कर रहा है। लेकिन ट्रम्प की नज़र सिर्फ भारत पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ़ कहा—“अगर चीन पर टैरिफ़ लगाया तो ऊर्जा कीमतें बढ़ जाएँगी। लेकिन भारत पर टैरिफ़ लगाना ज़रूरी है।” यह है अमेरिका का दोहरा मापदंड।
यही वजह है कि अमेरिकी कूटनीति के जानकार इवान फेगेनबाम कहते हैं—“अमेरिका कैसे चीन-विरोधी गठबंधन से भारत-विरोधी गठबंधन में बदल गया, यह अमेरिकी इतिहास की सबसे अनोखी कहानियों में से एक होगी।” और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन तक कह चुके हैं—“ट्रम्प का यह रवैया भारत को रूस और चीन से दूर करने के अमेरिका के दशकों पुराने प्रयासों पर पानी फेर देगा।”
अब आप सोचिए, क्या यह सब सिर्फ़ राजनीति है? नहीं। यह है एक पैटर्न। अमेरिका जब भी किसी एशियाई ताक़त से डरता है, भारत उसकी आंच में झुलसता है। 80 के दशक में जापान था, 2000 के दशक में चीन था, और 2025 में फिर से चीन है। लेकिन बीच-बीच में, अमेरिका हर बार भारत पर दबाव बनाने का मौका ढूँढ लेता है।
1989 का भारत और 2025 का भारत—दोनों अलग हैं। तब हमारे पास foreign currency reserves कम था, अर्थव्यवस्था जकड़ी हुई थी। आज हम दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन एक बात आज भी वही है—अमेरिका का टैरिफ़ हथियार। फर्क सिर्फ़ इतना है कि तब हमारे नेता कहते थे—“हम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के खिलाफ़ नहीं झुकेंगे।” और आज हमें भी वही दोहराना है।
क्योंकि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ़ लगाता है, तो इसका असर सिर्फ़ बड़े उद्योगपतियों पर नहीं होगा। इसका असर आपके और मेरे घर के बजट पर होगा। मोबाइल फोन महंगे होंगे, दवाइयाँ महंगी होंगी, पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ेंगी। और जब ये बढ़ेंगे, तो महँगाई आपके किचन तक पहुँच जाएगी।
तो सवाल यह है—क्या हम फिर वही गलती दोहराएँगे? क्या हम अमेरिका के ‘सुपर 301’ जैसे हथियारों से डरकर अपनी नीतियाँ बदलेंगे? या फिर हम अपनी प्राथमिकताओं पर अडिग रहेंगे? इतिहास हमें यही सिखाता है कि अमेरिका जब भी अपनी ताक़त दिखाता है, भारत को अपने आत्मविश्वास की परीक्षा देनी पड़ती है। 1989 में हमने यह परीक्षा दी थी। 1991 में हमने मजबूरी में बदलाव किए थे। और 2025 में फिर से यह परीक्षा हमारे सामने है।
Conclusion
अगर हमारे आर्टिकल ने आपको कुछ नया सिखाया हो, तो इसे शेयर करना न भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। आपके सुझाव और सवाल हमारे लिए बेहद अहम हैं, इसलिए उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर बनाने में मदद करती हैं।
GRT Business विभिन्न समाचार एजेंसियों, जनमत और सार्वजनिक स्रोतों से जानकारी लेकर आपके लिए सटीक और सत्यापित कंटेंट प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। हालांकि, किसी भी त्रुटि या विवाद के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य आपके ज्ञान को बढ़ाना और आपको सही तथ्यों से अवगत कराना है।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे GRT Business Youtube चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद!”